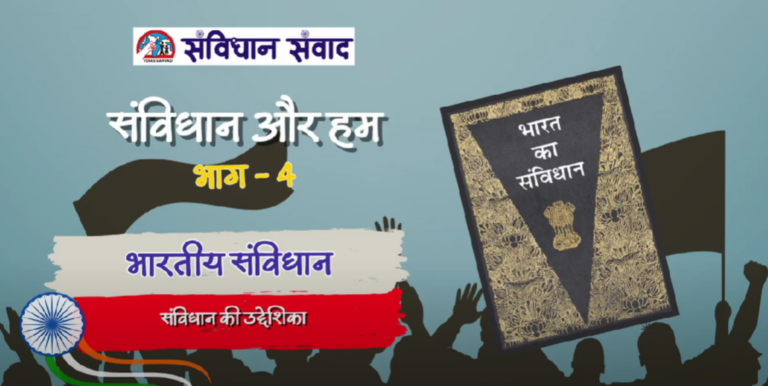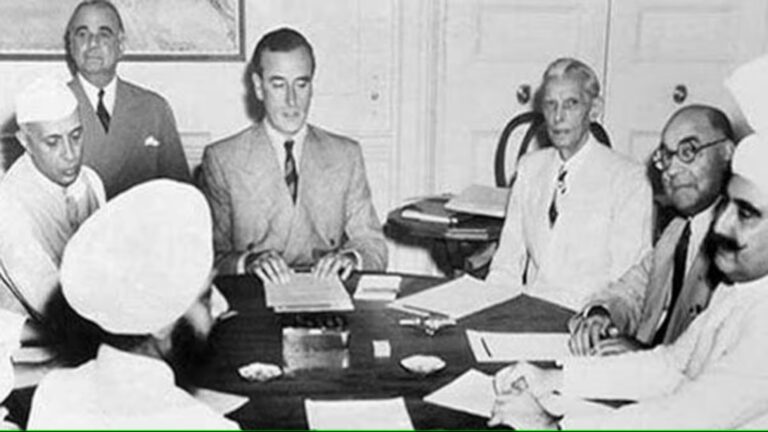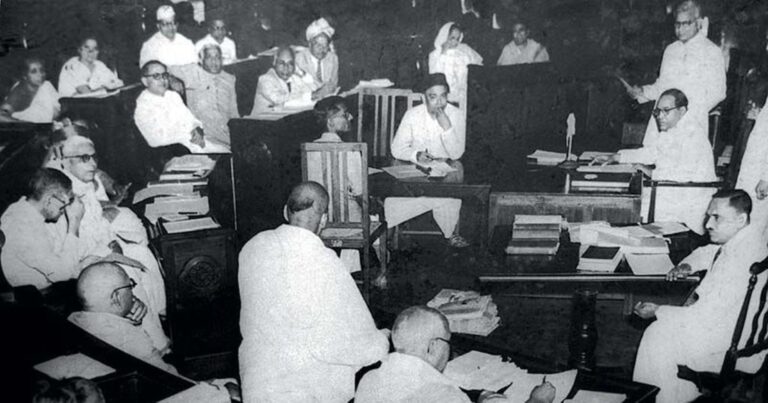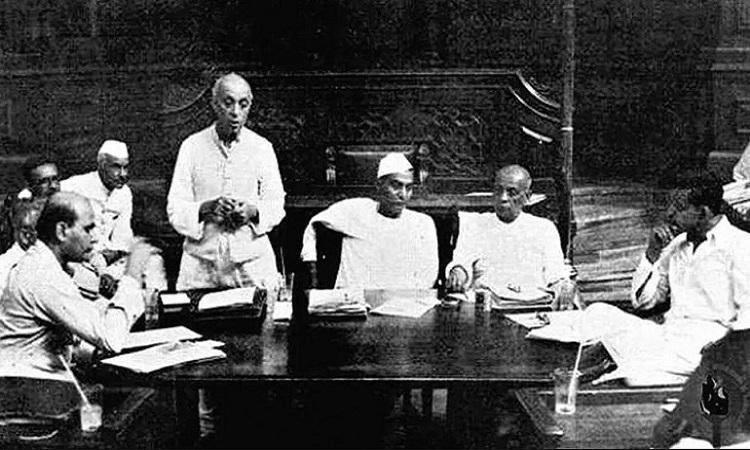बाइस जुलाई
तिरंगे को अपनाने का दिन
भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को औपचारिक रूप से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। 23 जुलाई को इसे पहली बार औपचारिक रूप से फहराया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक लंबी सुविचारित प्रक्रिया के बाद हमारे सामने आया। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के पहले देश की विभिन्न रियासतों और राज्यों के अपने-अपने ध्वज थे। विडंबना ही है कि संपूर्ण भारत को उसका पहला ध्वज साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन ने दिया।


सचिन कुमार जैन
संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।
बाइस जुलाई का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि वर्षों से भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में लंबे समय तक अगर किसी चीज की कमी खली थी तो वह था पूरे भारत का एक ध्वज। एक ऐसा ध्वज जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता हो। हमने तिरंगे को अपना तो बहुत पहले लिया था लेकिन 22 जुलाई 1947 को वह औपचारिक रूप से हमारा हुआ। अगले दिन यानी 23 जुलाई 1947 को न्यू काउंसिल हाउस (वर्तमान विधान भवन) में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से फहराया गया।
राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के पहले देश की विभिन्न रियासतों और राज्यों के अपने-अपने ध्वज थे। विडंबना ही है कि संपूर्ण भारत को उसका पहला ध्वज साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन ने दिया। नीले रंग के इस झंडे में बांयी ओर ऊपर यूनियन जैक बना था जबकि दाहिने हिस्से के बीच में ब्रिटिश क्राउन में स्टार ऑफ इंडिया का चित्र बना था।
राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा
किसी भी स्वतंत्र देश की पहचान को स्थापित करने में राष्ट्रीय ध्वज अहम प्रतीक होता है। सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने लगी थीं, ने राष्ट्रीय ध्वज न होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था, “विश्व युद्ध के बाद जिस दिन वार्सलीज़ में संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस दिन मैं संयोगवश पेरिस में थी। हर तरफ ख़ुशी थी। ओपेरा हाउस (संगीत भवन) सभी राष्ट्रों के झंडों से सजा था। एक प्रसिद्द अभिनेत्री रंगमंच पर आई, उसने फ्रांस के झंडे को अपने चारों और लपेट लिया। सभी दर्शकगण एक साथ खड़े हो गऐ और फ्रांस का राष्ट्रीय गीत – दी मार्सलीज़… गाया। तब एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा? मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही वह समय आने वाला है जब हमारा अपना झंडा भी होगा और राष्ट्रगीत भी।”
प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज
सात अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के प्रतिरोध में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पारसी बागान चौराहे पर एक झंडा फहराया। यह एक चौकोर तिरंगा झंडा था, जिसमें हरी, पीली और लाल/नारंगी पट्टियां थी। ऊपर की हरी पट्टी में आठ कमल के फूल आठ प्रान्तों के प्रतीक थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। गैर आधिकारिक रूप से यह पहला भारतीय ध्वज था।
सन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने क्रांतिकारियों के साथ पेरिस (फ्रांस) में लगभग इसी तरह का झंडा फहराया। पहली बार केसरिया रंग का इस्तेमाल इसी झंडे में हुआ था।
पिंगली वेंकैय्या की भूमिका
आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे पिंगली वेंकैय्या महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। 19 साल की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी से मिले। वहां से लौटने के बाद उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया और ऐसे ध्वजों की एक पुस्तक प्रकाशित की, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो सकते थे। वर्ष 1918-1921 के बीच वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के ध्वज की बात को उठाते रहे। भारत आने के बाद वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मिले और उन्हें विभिन्न देशों के ध्वजों पर अपने प्रकाशन दिखाए।
वेंकैय्या द्वारा बनाए गए शुरूआती झंडे में लाल और हरा रंग ही था। बाद में महात्मा गांधी और लाला हरदयाल के सुझावों के बाद इसमें शांति के प्रतीक के रूप में सफ़ेद रंग और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे को जोड़ा गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति ने इस ध्वज में लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग स्थापित कर दिया और इसमें रंगों के स्थान में भी परिवर्तन किया गया। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस ध्वज को अपना लिया।
सुरैय्या-बदरुद्दीन तैयबजी की भूमिका!
विद्वानों का एक समूह मानता है कि भारत का ध्वज तैयार करने में सुरैय्या तैयबजी और उनके पति बदरुद्दीन तैयबजी की अहम भूमिका थी। अंग्रेज इतिहासकर ट्रेवर रॉयले लिखते हैं, “भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी ने बनाया।” वहीं हैदराबाद के इतिहासकार कैप्टन पांडुरंग रेड्डी इसका श्रेय उनकी पत्नी सुरैय्या को देते हैं। संविधान सभा की ध्वज प्रस्तोता समिति में भी सुरैय्या तैयबजी का नाम शामिल है।
स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज
देश को आजादी मिलने से 23 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा, “भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा। जिसमें गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर-बराबर की तीन आड़ी पट्टियां होंगी। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरुप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ पर अंकित है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा।”
पंडित नेहरू ने कहा, ‘‘जब हम पराजित और निरुत्साहित हो जाते थे, तब इस झंडे का दर्शन आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिलाता था। मैं आपको यह झंडा भेंट करता हूं।”
चरखे की जगह चक्र
पंडित नेहरू के मुताबिक “चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था, उसका चक्र एक ओर था और तकुआ दूसरी ओर। यदि आप झंडे को दूसरी ओर से देखें तो चक्र इस ओर आ जाता था और तकुआ उस ओर। यह व्यावहारिक कठिनाई थी, विचार करने के बाद हमने यह सोचा कि इस महान चिह्न को रखा जाये, किन्तु थोड़ा परिवर्तन करना होगा। तब हमने चक्र को रखा और शेष भाग –तकुए और माल को नहीं रखा।”
जब महात्मा गांधी को पता चला था कि राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के चक्र के स्थान पर अशोक चक्र स्थापित किया गया है, तो वे दुखी हो गये थे हालांकि बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र अहिंसा का दैवीय कानून है।
अशोक चक्र ही क्यों?
चरखे की जगह चक्र रखने का निर्णय कर लिया गया तो अनेक चक्रों पर विचार हुआ परंतु अशोक की प्रमुख लाट के सिरे पर बना चक्र चुना गया क्योंकि यह देश की प्राचीन सभ्यता की निशानी है। नेहरू मानते थे कि भारतीय इतिहास में अशोक का काल वास्तव में अंतरराष्ट्रीय काल था। उस समय भारतीय राजदूत सुदूर विदेशों में गये, साम्राज्य और साम्राज्यवाद के रूप में नहीं, बल्कि शान्ति, सदाचरण और शुभकामना का संदेश लेकर।
कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने
यह जानना दिलचस्प है कि स्वयं कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं कांग्रेस के झंडे को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज न बना दिया जाये। दरअसल स्वतंत्रता आन्दोलन के समय प्रतीकात्मक ढंग से फहराये जाने वाले वाले झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में भी देखा जाता था। आज़ादी से कुछ महीने पहले दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मलेन हुआ। इस सम्मलेन में मंच पर एशिया के सभी देशों के झंडे और उनके प्रतीक चिह्न लगे थे लेकिन भारत ने वहां कोई झंडा नहीं लगाया क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में दल आधारित राजनीति के लिए कोई स्थान हो।
तिरंगा सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है!
यह दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता के एक वर्ग में यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गयी कि तिरंगे का केसरिया रंग हिंदुओं का तथा हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक है। देश के राष्ट्रीय ध्वज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गयी परंतु यह बात तथ्यात्मक दृष्टि से पूरी तरह गलत है।
पंडित नेहरू ने कहा था, ‘‘यह एक ऐसा झंडा है जिसके बारे में अलग-अलग बातें कही जाती हैं। कई लोग इसका गलत मतलब लगा बैठे हैं। वे इसे सांप्रदायिक नजरिये से देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि इसका कोई हिस्सा इस या उस समुदाय की नुमाइंदगी करता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब यह झंडा तैयार किया गया तो कोई सांप्रदायिक संकेत इसमें नहीं जोड़ा गया।’’
डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था, ‘‘यह झंडा हिन्दू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं, जैन, सिख, बौद्ध, किसी का नहीं; यह झंडा सारे हिन्दुस्तान का है।”
ध्वज को अपनाने से लेकर आज तक कई अहम घटनाएं घट चुकी हैं। ध्वज संहिता में संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हर भारतीय का मौलिक अधिकार बन चुका है। अब ध्वज की गरिमा का ध्यान रखते हुए हम इसे किसी भी दिन फहरा सकते हैं।