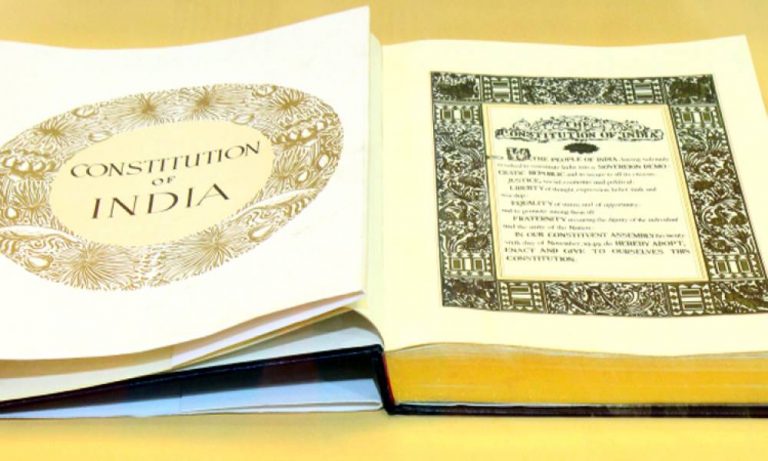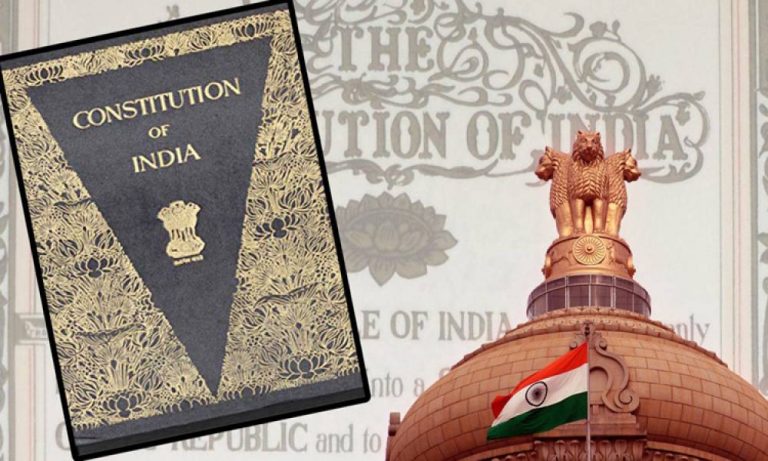व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में लोकतंत्र भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं
न्याय का अर्थ है नई दिशा की ओर बढ़ना ना कि अतीत की परिस्थितियों की ओर वापस लौटना। क्या हमें ऐसा होता दिखाई दे रहा है? वर्तमान परिस्थितियों तो जैसे प्रतिशोध आधारित न्याय की ओर इंगित कर रही हैं। क्या यह उचित है? संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही साथ शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन को स्थापित करता है। परंतु हमारी वर्तमान प्रणाली एकतरफा प्रतीत होती है?


चिन्मय मिश्र
गांधीवादी चिंतक एवं लेखक। समसामयिक मुद्दों के साथ सामाजिक सौहार्द्र पर विगत चार दशकों से लेखन एवं कार्य।
‘‘मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जूरी के निर्णय के बाद भी मैं खुद को बेगुनाह मानता हूं। वस्तुओं की नियति को उच्च शक्तियां निर्धारित करती हैं और हो सकता है परमात्मा की यही इच्छा हो कि जिस वस्तु के लिए मैं लड़ रहा हूं, वह मेरे जेल से बाहर रहने के बजाय मेरे तकलीफ उठाने पर अधिक फूले फले।”
– बाल गंगाधर तिलक
बंबई उच्च न्यायालय के केंद्रीय कक्ष में इस पट्टिका का अनावरण करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एमसी चागला ने कहा था कि “तिलक की स्मृति में आज सुबह इस पट्टी के अनावरण का जो सौभाग्य मुझे मिला, उसकी तुलना किसी और सम्मान या प्रतिष्ठा से नहीं की जा सकती है। 12 साल की अवधि में 2 बार इस कक्ष में वे अभियुक्त के कटघरे में खड़े हुए और उन्हें दोनों ही बार कारावास का दंड सुनाया गया। भारत के इस महान और विख्यात सपूत को इन सजाओं द्वारा जो तकलीफ दी गई उसका प्रायश्चित करने के लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं।” न्यायमूर्ति चागला ने कहा था कि यह इतिहास पर धब्बा है। ये दंड न्याय का तकनीकी अनुपालन भर थे। गौरतलब है तिलक को धारा 124 (अ) देशद्रोह व 153 (अ) के अंतर्गत सजा दी गई थी। अपने संबोधन में वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी कहते हैं कि, “हमारे समकालीन हम पर जो फैसला सुनाते हैं, हमारा समय हम पर जो निर्णय सुनाता है, उसका अधिक मूल्य नहीं होता। मूल्यवान होता है इतिहास का अपरिहार्य निर्णय और इतिहास का अपरिहार्य निर्णय है कि आजादी और देशप्रेम की आवाज दबाने वाली यह दोनों सजाएं निंदनीय हैं। तिलक ने जो किया वह देश के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति का न्याय संगत अधिकार है। यह दोनों सजाएं विस्मृत हो चुकी हैं और तिलक की महानता स्थापित हो चुकी है।”
ठीक इसी समय सन 1908 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक एक्ट का जबरदस्त विरोध करते हुए कह रहे थे, “मेरे हिसाब से यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत एशियाटिक एक्ट को रद्द करने से हों और न ही यह कि एशियाटिक एक्ट के रद्द होने से यह बात समाप्त हो जाएगी। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि इस उपनिवेश की सरकार आज इस कानून को रद्द करने के लिए तैयार है, यह हमारी आंखों में धूल झोंकना ही है क्योंकि वे इसके बाद और अधिक कठोर वह अपमानजनक कानून लाएंगे। लेकिन मैं इससे स्वयं यह सीखना चाहता हूं और अपने देशवासियों को सिखाना चाहता हूं कि अभी हम भले ही कितने असहाय नजर आ रहे हों, लेकिन हमें सशक्त बनना होगा हमें समझना होगा कि हम इस महान सृष्टि का एक हिस्सा है और इन राजाओं के बजाय वह ही है जो हमारी नियति तय करता है। हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए। और चाहे जैसा भी कानून पारित हो यदि वह अन्यायपूर्ण है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसे अपने पर चढ़ने नहीं देना चाहिए। (सामान्य अनुवाद)
इन दोनों घटनाओं के करीब 115 वर्ष बाद और आजादी के 75 वर्षों बाद भारत में आज वे सभी धाराएं लागू हैं जिनके आधार पर तिलक को जेल भेजा गया था। इतना ही नहीं अब तो उससे भी अधिक दमनकारी, खतरनाक व जनविरोधी कानून भारत में प्रचलित हैं और लगातार उन्हें स्वीकार्य भी बनाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामले में जेल में निरुद्ध सभी बुद्धिजीवी, इसी तरह के दमनकारी कानूनों में निरुद्ध हैं। इस बीच फादर स्टेन स्वामी स्वर्ग सिधार चुके हैं। अन्य में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब है। सुधा भारद्वाज व गौतम नवलखा भी बीमार हैं। सुधा भारद्वाज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ काम करती हैं, इस संगठन के प्रणेता शहीद शंकर गुहा नियोगी द्वारा मार्च 1991 में दुर्ग जेल में लिखी कविता है:
मैं हूं यहां अकेला
जो जुटे हुए हैं खेतों में
कारखानों में
व्यस्त हैं जुलूसों में
उनसे दूर यह अकेलापन
क्या नहीं है असंगत?
हम आजादी का अमृत महोत्सव बड़े जोर शोर से मना रहे हैं, परंतु क्या यह आवश्यक नहीं है कि आजादी के जश्न में उन्हें भी शामिल किया जाए जो हमसे असहमत हैं, सरकार का विरोध देश विरोध का पर्याय नहीं हो सकता। भारतीय लोकतंत्र की सार्थकता तो तभी सिद्ध होगी कि आजादी के 75 वें वर्ष में उन लोगों से राजनीतिक स्तर पर सीधी बात की जाए जो वर्तमान शासन व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। इस दौरान उनसे भी बात की जानी चाहिए जिन्होंने हिंसात्मक विकल्प को चुनने की गलती की है। परंतु हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? शायद हम इतना नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि असहमत से आंख मिलाकर बात कर सकें। कानून और पुलिस किसी भी समस्या को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, विशेषकर तब जबकि समस्या राजनीतिक हो। नियोगी की एक और कविता की पंक्तियों पर गौर करिए:
अध्यादेश पर अध्यादेश
संशोधन पर संशोधन
धौंस… संत्रास… आतंक
पूरा देश बना जेलखाना
पुलिस हुई विचारकर्ता
60 करोड़ नागरिकों का हाल बेहाल
यही तो है 26 जून का आपातकाल।
आपातकाल को लगाए और बीते करीब 50 वर्ष बीतने आए। परंतु क्या लगता है, आपातकाल चला गया या उसका कोई नया नामकरण हो गया है?
गौरतलब है न्याय का अर्थ है नई दिशा की ओर बढ़ना ना कि अतीत की परिस्थितियों की ओर वापस लौटना। क्या हमें ऐसा होता दिखाई दे रहा है? वर्तमान परिस्थितियों तो जैसे प्रतिशोध आधारित न्याय की ओर इंगित कर रही हैं। क्या यह उचित है? संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही साथ शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन को स्थापित करता है। परंतु हमारी वर्तमान प्रणाली एकतरफा प्रतीत होती है? क्या कानून संविधान के ऊपर है?
वर्तमान परिस्थितियां हमें यह सोचने पर बातें कर रही हैं कि क्या दया और प्रेम न्याय से अलग या इसके विपरीत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं और उसके बाद सजा पर विचार करते हैं। वे अपने निर्णय में दयावश दंड देने की अवधि व मात्रा पर भी विचार करते ही हैं| हम न्याय/कानून की जिस नई व्यवस्था को अपना चुके हैं वह धार्मिक (बाइबिल) न्याय से उभरी थी और प्रेम उसका अनिवार्य हिस्सा था। वास्तविकता भी यही है कि प्रेमपूर्वक किया गया न्याय मनुष्य को मात्र दंडित करने के बजाय उसे ठीक करने में विश्वास रखता है। आज इस विचार को न केवल नकारा जा रहा है बल्कि पूरी ताकत से यह प्रचार किया जा रहा है कि जैसे क्रूरता वर्तमान न्याय व्यवस्था की एक अनिवार्यता बन गई है या बनती जा रही है। आज मृत्युदंड से कम की मांग नहीं होती है।
11वीं – 12वीं शताब्दी में बदली परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान कानून व्यवस्था ने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया। धीरे-धीरे राज्य पीड़ित की ओर से खड़ा होने लगा और अंततः पीड़ित की स्थिति एक फुटनोट तक सीमित होकर रह गई। यह भी तय है कि निजी न्याय और राज्य द्वारा किए जा रहे न्याय में फर्क तो होना चाहिए। परंतु राज्य उस महीन सीमा रेखा का लगातार अतिक्रमण करता चला जा रहा है। यह सब वैश्विक स्तर पर भी हो रहा है। आरोपी को सार्वजनिक तौर पर क्रूरता व पीड़ा से बचाने के लिए ही तो कारागारों की स्थापना की गई थी। यह एक ऐसा विचार था जिसके अंतर्गत अभियुक्त को अमानुषिक यातना से बचाया जाना सुनिश्चित किया जाना था। परंतु आज क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? निजी व सार्वजनिक दर्द के स्थान पर एकांत स्थान को यातना स्थल बनाया जा रहा है। जेल के भीतर एक और जेल। जेल के भीतर अंडा सेल जैसे उदाहरण यह बता रहे हैं कि यह व्यवस्था किस कदर असफल और राज्य व सरकार केंद्रित होती जा रही है। जेल सुधार मात्र भौतिक सुविधाओं से बेहतर होने तक ही सीमित नहीं है, यह इसमें इससे बहुत आगे की स्थिति है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि राजनैतिक असहमति को सिर्फ कानूनी नजरिए से कैसे शांत किया जा सकता है? राजनीतिक पहल क्यों नहीं प्रारंभ की जा रही? अमृता प्रीतम लिखती हैं:
खुदा रहम करे इस घर पर
जहां कभी रांझा बजता था
यहां खेड़ा की पदचाप सुनाई देती है।
वहीं पंजाबी के ही एक अन्य कवि मोहनजीत कहते हैं:
मैं यहीं जन्मा
पैदा हुआ
मैं इस धरती का गौरव
मैं ही इसका शोक गीत हूं।
रांझा की जगह खेड़ा का आना और गौरव का शोकगीत में बदल जाना वास्तव में बेहद शोचनीय स्थिति है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तकरीबन प्रत्येक राज्य फिर वे भाजपा शासित हों या विपक्ष शासित दमनकारी कानूनों को अपना खेवनहार बनाये हुए हैं। जनता का एक हिस्सा स्तब्ध है तो दूसरा निर्लिप्त। दोनों ही परिस्थितियां एक जीवंत लोकतंत्र के लिए प्राणघातक ही हैं। क्या विपक्ष शासित राज्य इस ओर पहल कर सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपनी पूरी शिद्दत से स्थापित हो सके। हमें याद रखना चाहिए कि पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में लोकतंत्र को भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का पेगासस मामले में दिया गया निर्णय इसका सीधा-सीधा उदाहरण है। नियोगी लिखते हैं:
रो मां रो
नहीं तो तेरे बच्चे का दर्द
मेरे देशवासियों के सीने में बैठ जाएगा।
केंद्र सरकार को चाहिए कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक सकारात्मक अभियान चलाए। दमनकारी कानूनों में निरुद्ध राजनीतिक कैदियों को पैरोल पर रिहा कर उनसे उच्च स्तर पर चर्चा की जाए। असहमति को पनपने दिया जाए जिससे कि वह फटने की स्थिति में ना पहुंच पाए। यह एक कठिन निर्णय है लेकिन समाधान तो इसी से निकल सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में एक भी राजनीतिक बंदी का होना, हमारी असफलता का द्योतक है। अंत में शंकर गुहा नियोगी की इन पंक्तियों पर गौर करिए:
सात कटीले तार
अब तक छूता था मजदूर
जब कभी इन तारों को
होता था लहूलुहान उसका शरीर
अब वह बन गया
सितार के सात तार
पैदा करेगा मजदूर आंदोलन
इन तारों से आवाज।