संविधान पर लगे आरोपों का सीधे सामना करने का वक्त
हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे सामने यह चुनौती है कि हम अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों को किस प्रकार अपनाएं। यह आवश्यक है कि संविधान पर लगने वाले आरोपों का सीधे-सीधे सामना किया जाए। अक्सर इन आरोपों को राजनीतिक मतभेद और विचारधाराओं के टकराव के नजरिए से देखा जाता है। इन सवालों को एक रचनात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए एक बुनियादी मानवीय सत्य के आधार पर इन पर विचार करें। एक बेहतर समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है लेकिन इस प्रयास में हाथ लगने वाली नाकामियों से घबराए बिना हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए।
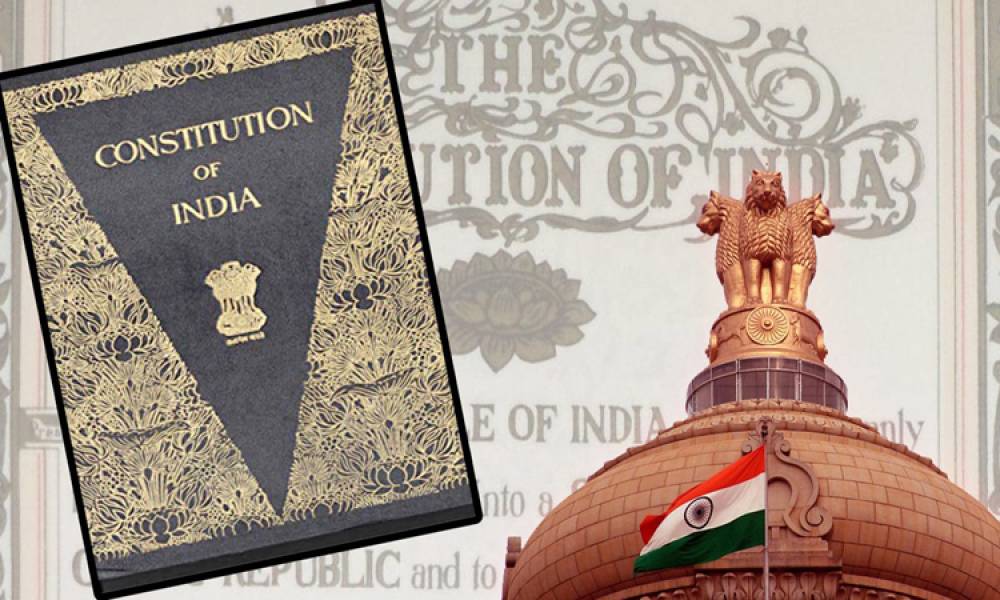

रजनी बक्शी
स्वतंत्र पत्रकार और लेखक। भारतीय सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर निरंतर लेखन।
कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र के कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारत के संविधान पर एक अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य था समाज में भारतीय संविधान के मूल्यों को लेकर जानकारी बढ़ाना और उन पर चर्चा शुरू करना। मैंने भी इस अभियान की एक दिन की कार्यशाला में भाग लिया और वहां मुझे कई नई बातें सीखने को मिलीं। मिसाल के तौर पर इससे पहले मुझे यह पता नहीं था कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, तब संविधान सभा में इस बात को लेकर गहरी चर्चा हुई थी कि यह संविधान हमें कौन दे रहा है?
उस समय एक विचार यह सामने आया कि संविधान हमें भगवान की असीम कृपा से मिल रहा है। यह भी सोचा गया कि शायद महात्मा गांधी का नाम आना चाहिए, कि संविधान हमें उनके नेतृत्व से मिला है। ऐसे तमाम विचारों पर विमर्श हुआ और आखिर में इन सबको छोड़कर यह तय किया गया कि हम भारत के लोग खुद अपने आप मिलकर इन मूल्यों के प्रति संकल्प लेते हैं। इन मूल्यों के सार तत्व हैं- न्याय, आजादी और समानता। स्वयं के साथ किया गया यह संकल्प ही आधुनिक भारत की नींव है।
परंतु इस बात को लेकर आज भी कई तरह के विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। विवाद का एक मुद्दा यह भी है कि हमारा संविधान वास्तव में ‘भारत के लोगों’ ने नहीं बनाया। इस आलोचना के तहत कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले तो उच्च वर्ग और उच्च जाति के कुछ लोग थे, वे भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। दूसरा आरोप यह है कि ‘न्याय, आजादी और समानता’ के मूल्य विदेशी हैं जो दरअसल पश्चिम के देशों के इतिहास और संस्कृति से निकले हुए हैं। कहा जाता है कि ये मूल्य भारत के बहुमुखी समाज पर आधारित नहीं हैं।
हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब यह आवश्यक है कि इन आरोपों का सीधे-सीधे सामना किया जाए। अक्सर इन आरोपों को राजनीतिक मतभेद और विचारधाराओं के टकराव के नजरिए से देखा जाता है। मेरा प्रयास है कि इन सवालों को एक रचनात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए एक बुनियादी मानवीय सत्य के आधार पर इन पर विचार करें। वह सत्य यह है कि हर इंसान इज्जत की जिंदगी चाहता है और चाहता है कि वह प्रसन्न रहे।
पहले इस सवाल को संबोधित करते हैं कि क्या ‘हम भारत के लोग’ में वास्तव में हम सभी भारतीय शामिल हैं? यहां एक बात साफ कर दूं कि हमें इस सवाल को इस तरह नहीं देखना है कि संविधान निर्माण या उसे स्वीकार करने वालों में हमारे परिवार के लोग शामिल थे या नहीं। जब मैं अपने परिवार पर विचार करती हूं तो मुझे याद आता है कि मैंने अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों में बदलते भारत के प्रति कई अलग-अलग भाव देखे थे। कुछ बुजुर्ग मानते थे कि सभी जातियों के लोग बराबर नहीं होते और उनमें बराबरी की बात करना गलत है। ऐसा सोच रखने वाले बुजुर्गों ने ही हम बच्चों के मन में सफाई कामगारों के प्रति छुआछूत की भावना डाल दी। हालांकि यह कोई इकलौता नजरिया नहीं था बल्कि उस समय तमाम अन्य नजरिए भी थे जिन्होंने हम बच्चों को प्रभावित किया।
मेरे माता-पिता की उम्र के परिजन जो 1950 और 1960 के दशक में युवा थे, वे इन पुराने विचारों से सहमत नहीं थे। वे हमें सिखाया करते थे कि गैरबराबरी और जातिभेद के विचारों को बदलने का वक्त आ गया है। वे हमें बताते कि हमारे समाज ने आजादी की लड़ाई केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं लड़ी थी बल्कि नया भारत बनाना भी उसका लक्ष्य था। अगर संविधान का उल्लेख न भी किया जाए तो भी हमें यह साफ तौर सिखाया गया कि आज़ाद भारत के मूल्य हैं- न्याय, आजादी, समानता और भाईचारा या बंधुत्व। मेरे परिवार में दूर-दूर तक ऐसा कोई नहीं था जिसकी संविधान निर्माण में कोई भूमिका रही हो। परंतु हमारे माता-पिता ने और उनके हम उम्र लोगों ने हमें हमेशा यही सिखाया कि न्याय, आज़ादी और समानता के बल पर ही भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा।
उस दौर की फिल्मों में भी बार-बार यह दोहराया जाता था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की डगर कठिन है लेकिन हमें इस रास्ते पर हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं हमें हार नहीं माननी है और पीछे नहीं हटना है। यह माहौल केवल गांधी-नेहरू या कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं बना था। वह परिवर्तन का दौर था जहां आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष कई स्तरों पर चल रहा था। बीसवीं सदी के आरंभ में हुई क्रांतियों ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। आज़ाद भारत ने वामपंथ को नहीं अपनाया लेकिन आर्थिक न्याय का सपना हमारी फिल्मों, गीतों, कहानियों और कविताओं में हमेशा मौजूद रहा। वह हमारे अनेक गैरदलीय राजनैतिक संघर्षों में भी चमकता रहा।
रचनात्मक ढंग से परिभाषाओं को दें नया रूप
इस बीच यह सवाल बार-बार सिर उठाता रहा कि क्या आजादी, न्याय और समानता वाकई ‘बाहरी मूल्य’ थे? कहा जाता है कि पश्चिम में ‘समानता’ की जो परिभाषा है वह भारत के इतिहास और संस्कृति में नहीं दिखती। परंतु सच यह है कि समानता की आधुनिक परिभाषा पश्चिम तक सीमित नहीं है। अगर हम भारतीय, इतिहास को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो साफ नजर आता है कि समाज के स्थूल और सूक्ष्म पहलू में सामाजिक रिश्तों की विडंबना की उथलपुथल सदियों से चली आ रही है। हमारे लिए उस इतिहास को समझना आवश्यक है लेकिन हमारा वर्तमान और भविष्य केवल उसी समझ तक सीमित या उस पर निर्भर नहीं है। हम ऐसी परिभाषाओं को रचनात्मक ढंग से नया रूप दे सकते हैं।
अब वक्त आ गया है कि हम समानता को रचनात्मक और करुणामयी रूप में समझें और अपनाएं। ‘समानता’ को ‘विदेशी’ बताना आम जनमानास की अभिलाषा को नकारना होगा जो एक तरह से अमानवीय भी है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो भारतीय संविधान को संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानता हो लेकिन सच तो यही है कि संविधान को लेकर जो विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं उनके पीछे एक गहरा और खतरनाक सोच है। समाज का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि कई लोग उसे बांटकर देखने लगे हैं। उन्हें समाज ‘हमारे’ और ‘दूसरे’ लोगों में विभाजित नजर आने लगा है। इसका सबसे तीव्र रूप ‘हिन्दू’ और ‘मुसलमान’ विभाजन का है लेकिन यह वहीं तक सीमित नहीं है।
इस मानसिकता के शिकार लोगों को लगता है कि संवैधानिक हक ‘अपनों’ के लिए हैं ‘दूसरों’ के लिए नहीं। यह भी सुनने में आता है कि संवैधानिक हक सिर्फ उनके लिए हैं जो देश-भक्त हैं। परंतु यहां सवाल यह है कि देशभक्त या देशद्रोही का निर्धारण किस आधार पर होगा? संविधान के उसूलों को इस प्रकार मनमर्जी से मानने या न मानने की वजह केवल कथित ‘दूसरों’ को मुश्किल नहीं होगी बल्कि यह खतरा सबके लिए है। एक बार अगर संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो जाती है तब पता नहीं निरंकुश सत्ता कब किसको अपना शिकार बना ले। हाल ही में न्यायालयों ने कई अहम फैसलों में ऐसा रुख अपनाया जिससे यह नतीजा निकला कि जो लोग न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, वे खुद न्याय की मांग करने पर कठघरे में खड़े कर दिए गए।
इन हालात में केवल इतना काफी नहीं कि युवा पीढ़ी को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी दी जाए और उनमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाए। इससे भी आवश्यक यह है कि ‘हमारे’ और ‘दूसरे’ वाले माहौल को बदला जाए, इस मानसिकता को परिवर्तित किया जाए।
इसे कई तरह से अंजाम दिया जा सकता है। एक तरीका तो यही है कि संवैधानिक मूल्यों के बल पर समाज में जो बेहतरी आई है, उसे चिह्नित करें और उससे प्रोत्साहित हों। ज्यादातर अवसरों पर हम इसका उलट करते हैं और इन मूल्यों की नाकामियों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसमें दो राय नहीं कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन बेहद शर्मनाक स्तर तक पहुंच गया है लेकिन अगर हम केवल कमियों और नाकामियों की बात करें तो उन मूल्यों को लेकर समाज का मनोबल कैसे बढ़ेगा?
यह चेतना भी बढ़ानी होगी कि संवैधानिक मूल्यों को जीवन में किस तरह उतारा जाए। यह काम आसान नहीं है लेकिन संभव अवश्य है। इस चेतना से हमें शक्ति प्राप्ति होगी और निराशा से बचाएगी। सदियों पहले भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक प्रवाह में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ‘वसुधैव कुटंबकम’ ही जीवन का सत्य है। अगर उस सत्य को अधूरा जिया गया या नकारा गया तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह झूठा हो गया। वह सत्य कायम है और एक चुनौती के रूप में आधुनिक भारत के समाज को ललकार रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्य उसी सत्य को आवाज दे रहे हैं।
मूल्यों को लागूू करने का एक उदाहरण
एक उदाहरण प्रस्तुत है जो बंधुत्व के मूल्य को बताता है और प्रेरणा देता है कि कैसे हम इस मूल्य का लेकर काम कर सकते हैं। मुझे यह किस्सा राजस्थान के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी ने सुनाया था। उन्होंने बताया कि राजस्थान के कई इलाकों में एक समय यह समस्या होने लगी कि जब भी दलित जाति का कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठकर धूमधाम से बारात निकालता तो तथाकथित ‘ऊंची’ जाति के कुछ नौजवान उसकी बेइज्जती करते और उसे घोड़ी से जबरन उतार देते। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं थ कि दलित दूल्हा घोड़े पर बारात निकाले।
भंवर और उनके साथियों ने युवाओं से बात करना मुनासिब नहीं समझा और उस जाति की समाज सभा से संपर्क किया तथा संवाद की प्रक्रिया आरंभ की। संवाद सफल रहा और उस जाति सभा ने अपने को समझाया कि कि किसी समाज के व्यक्ति को पीड़ित करना, या उसके साथ झगड़ा करना गलत है। यह मूल मानवीय भाव पर आधारित संवाद जब सफल हुआ तो भंवर ने उस जाति सभा के नेता को संविधान की पुस्तक भेंट की। उस नेता ने कहा कि आज तक वह मानते थे कि संविधान के कारण ही ‘उच्च’ जातियों ने बहुत कुछ खोया लेकिन अब वह संविधान को नए नजरिए से देखते हैं और उसे पढ़ेंगे।
हम यह नहीं कह सकते कि गांव में दलित दूल्हों का उत्पीड़न पूरी तरह बंद हो गया लेकिन कुछ बदलाव अवश्य आया। आशा यही है कि आने वाले वर्षों में यह दुव्यर्वहार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आवश्यक नहीं कि ऐसा संवाद हमेशा सफल साबित हो। कई बार इसकी नाकामी अपने साथ दु:खद परिणाम भी लेकर आती है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि संवाद के जरिए बंधुत्व के प्रयास जारी हैं और इस तरह हमारे संवैधानिक मूल्य भी जीवित हैं।
संविधान हमें राह दिखाता है लेकिन रास्ता तो हमें ही तय करना है। इस मार्ग पर कायम रहना ही अपने आप में लक्ष्य है। हर कदम, हर पड़ाव पर सफलता मिलती है या विफलता यह हमारे हाथ में नहीं है। हौसले बुलंद रखना अवश्य हमारे हाथ में है।






