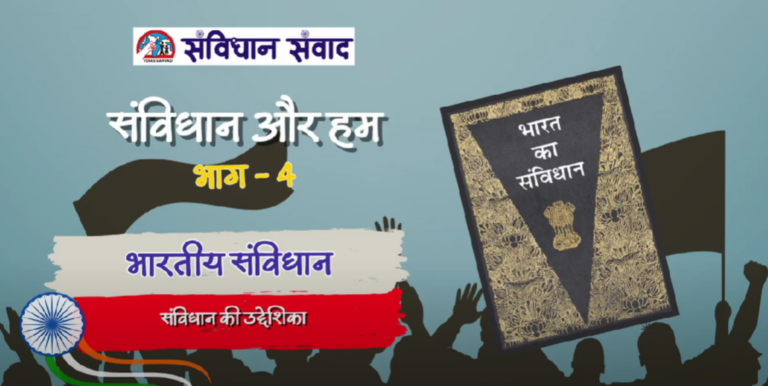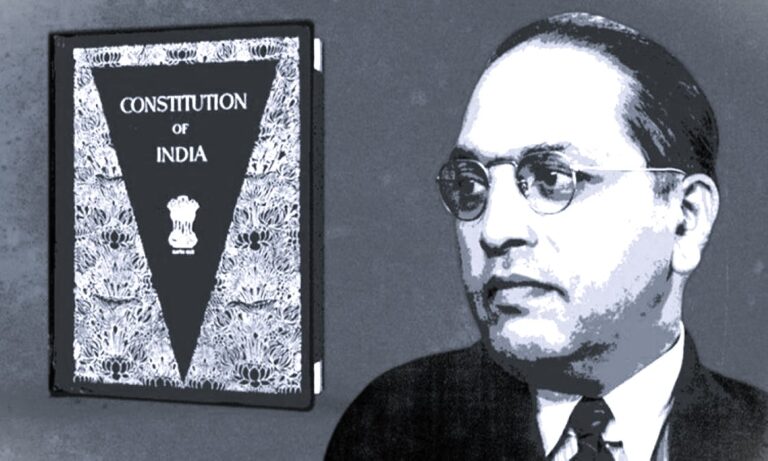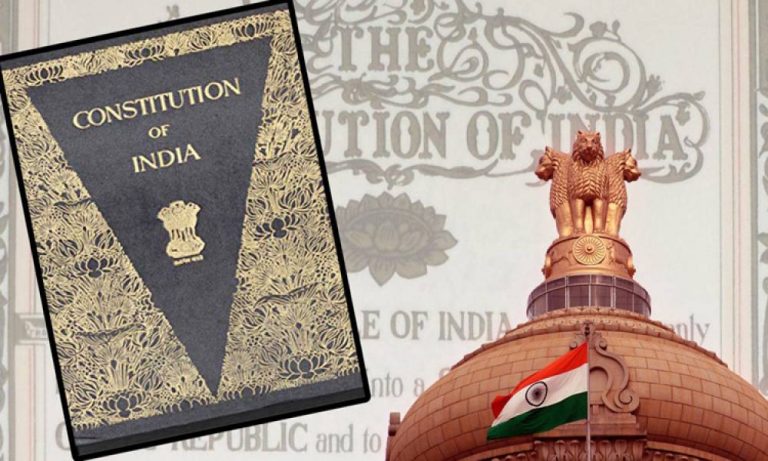जन्मदिन पर विशेष
संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर का अंतिम संबोधन
आज डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती है। यह उपयुक्त अवसर है कि हम 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए डॉ. अम्बेडकर के अंतिम भाषण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें। अपने इस भाषण में उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की कामयाबी के लिए जरूरी तत्वों पर बात की है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा समता और बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों की जरूरत को रेखांकित करता और इनका विश्लेषण करता हुआ उनका यह भाषण बताता है कि भारत के भविष्य की राह को लेकर वह क्या सोचते थे।


सचिन कुमार जैन
संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।
भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को अक्सर संविधान निर्माता कहा जाता है। परंतु सच तो यह भी है कि वह संविधान सभा के सलाहकार बी.एन.राऊ, मसौदा समिति के सदस्यों तथा संविधान के मुख्य मसौदाकार एस.एन. मुखर्जी के योगदानों के लिए उनके शुक्रगुजार थे।
संविधान के क्रियान्वयन को लेकर भी उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट थी। वह मानते थे कि किसी संविधान का क्रियान्वयन पूरी तरह संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान सभा में दिए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, “मैं यह महसूस करता हूं कि संविधान चाहे जितना बेहतर हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत हुए तो वह बुरा संविधान साबित होगा। इसी तरह एक संविधान चाहे जितना बुरा हो लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो वह अच्छा संविधान साबित होगा।”
उनका मानना था कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में राज्य को एक ढांचा और कुछ अंग प्रदान कर सकता है लेकिन इन अंगों को काम करने के लिए जिन कारकों की जरूरत है, वे हैं जनता और ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें अपनी इच्छाओं और राजनीति को पूरा करने के लिए वे साधन के रूप में प्रयोग में लाएंगे।
संसदीय लोकतंत्र के पैरोकार
डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में संविधान की आलोचना के बारे में भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि संविधान की आलोचना करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी प्रमुख रहे हैं। वास्तव में इन दोनों दलों ने संविधान की आलोचना क्यों की? क्या उन्हें भारतीय संविधान दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में कमजोर प्रतीत हो रहा था? वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा संविधान चाहती थी जिसमें सर्वहारा का दबदबा हो। कम्युनिस्ट पार्टी को संसदीय लोकतंत्र पर आधारित संविधान रास नहीं आ रहा था। वहीं डॉ. अम्बेडकर के मुताबिक सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसा संविधान चाहती थी जो उन्हें बिना कोई हर्जाना चुकाए निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की छूट दे। इसके अलावा समाजवादी धड़ा चाहता थाकि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर कोई बंधन लागू नहीं हो।
डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वह यह नहीं कहते कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत राजनीतिक लोकतंत्र के लिए एकमात्र आदर्श व्यवस्था है। संविधान सभा में हुई सार्थक चर्चाओं को लेकर अम्बेडकर की राय हमें जरूर यह बताती है कि वह इस व्यवस्था के हामी थे। उन्होंने अपने भाषण में कहाथा, “अगर इस संविधान सभा में हर सदस्य या हर समूह का अपना एक कानून होता तो चारों ओर अफरातफरी का माहौल होता। तब मसौदा समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता।”
उन्होंने संविधान सभा में असहमति का स्वर रखने वाले सदस्यों को भी रेखांकित किया और कहा, “खुशकिस्मती से संविधान सभा में कुछ विद्रोही स्वभाव के लोग भी रहे। इनमें श्री कामथ, डॉ. पीएस देशमुख, श्री सिधवा, प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना, प्रोफेसर के.टी. शाह, पंडित हृदय नाथ कुंजरू और पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे लोग शामिल हैं।”
उन्होंने खुले दिल से कहा कि अगर मैं उनके सुझावों को शामिल करने को तैयार नहीं था तो इसका यह मतलब नहीं कि संविधान सभा में उनकी सेवाओं के मूल्य को कम करके आंका जाए। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं।
केंद्रीकरण का प्रश्न
अक्सर यह बात भी उठती है कि भारतीय संविधान का बहुत अधिक केंद्रीकरण किया गया और केंद्र को शक्तिशाली बनाते हुए राज्यों को बहुत सीमित अधिकार सौंप दिए गए। इस विषय पर डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह विचार न केवल अतिरंजित है बल्कि यह संविधान को लेकर गलत समझ पर आधारित विचार भी है। उन्होंने कहा कि जहां तक केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात है तो हमें इनके पीछे के बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म यानी संघवाद का बुनियादी सिद्धांत यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकारों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है। यह काम केंद्र के किसी कानून के जरिये नहीं बल्कि सीधे संविधान के माध्यम से किया गया है। संविधान के अधीन राज्य किसी भी तरह से अपने विधानों या कार्यकारी प्राधिकार के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। केंद्र और राज्य इस मामले में एक समान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रकृति वाले संविधान को केंद्रीकृत संविधान कहना सही नहीं। इसी प्रकार यह कहना भी पूरी तरह गलत है कि राज्यों को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है।
राज्यों पर केंद्र के दबदबे के आरोप के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान की आलोचना करने के बजाय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात तो यह कि ये अधिकार संविधान की सामान्य विशेषता में नहीं आते। उनका इस्तेमाल और क्रियान्वयन केवल आपात परिस्थितियों तक सीमितहै। उन्होंने कहा कि आपात स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियां देना लाजिमी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कहीं अधिक जटिल समस्याएं पैदा हो सकतीहैं।
उन्होंने ‘द राउंड टेबल’ पत्रिका को उद्धृत करते हुए कहा, “राजनीतिक व्यवस्थाएं अधिकारों और कर्तव्यों की जटिल व्यवस्था होती हैं जो इस प्रश्न पर निर्भर होती हैं कि नागरिक की निष्ठा किसके प्रति और किस हद तक हो? सामान्य समय में यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सब कुछ सहजता से चलता है। परंतु मुश्किल के समय यह प्रश्न उठता है कि नागरिक की निष्ठा किस प्राधिकार के प्रति हो?”
ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि मुश्किल के समय नागरिकों की निष्ठा केंद्र के प्रति होनी चाहिए क्योंकि वह एक साझा लक्ष्य की ओर तथा देश के समग्र हित में काम कर सकता है।
आज़ाद भारत की तकदीर
भारत के भविष्य के बारे में उन्होंने कहा, “भारत एक स्वतंत्र देश बन गया है। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा। वह बरकरार रहेगी या फिर वह उसे दोबारा गंवा देगा? ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश था ही नहीं। सवाल तो यह है कि एक बार आज़ादी गंवाने के बाद क्या वह दोबारा उसे गंवा सकता है? यह प्रश्न मुझे बहुत अधिक बेचैन करता है। ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि भारत ने अपनी आजादी अपने ही लोगों की धोखेबाजी और गद्दारी के कारण गंवाई। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के समय राजा दाहर के सेनापतियों ने मोहम्मद बिन कासिम के लोगों से रिश्वत ली और अपने राजा का साथ छोड़ दिया। जयचंद ने पृथ्वीराज पर हमले के लिए मोहम्मद गोरी को बुलाया। जब शिवाजी हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ रहे थे तब अन्य मराठा और राजपूत राजा मुगल बादशाहों की ओर से लड़ रहे थे।”
उनकी चिंता थी कि क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? उन्होंने कहा कि अगर हम जाति और धर्म को देश से ऊपर रखेंगे तो इसमें शक नहीं कि एक बार फिर हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।
लोकतंत्र पर विचार
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत लोकतंत्र की अवधारणा से परिचित नहीं है। एक समय था जब भारत में ढेर सारे गणराज्य थे। भारत की परंपरा संसदीय प्रक्रियाओं की परंपरा से परिचित रही है। बौद्ध भिक्षु संघों का अध्ययन बताता है कि संघों में भी संसदीय व्यवस्था और प्रक्रियाएं थीं। वहां बैठक व्यवस्था, प्रस्ताव, समझातों, कोरम, मतगणना जैसी तमाम लोकतांत्रिक परंपराएं थीं जो आधुनिक लोकतंत्र का भी हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि भारत एक बार अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली गंवा चुका है और सवाल यह है कि क्या वह दोबारा इसे गंवा सकता है? उन्होंने कहा कि भारत जैसे नवजात लोकतांत्रिक देश में तानाशाही का खतरा एक वास्तविक खतरा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक तौर तरीकों का दामन थामे रखना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक रास्तों को ही अपनाना चाहिए। उनके रहते असंवैधानिक मार्ग अपनाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिलकी चेतावनी को याद किया जो लोकतंत्र को पसंद करने वालों से कहती है कि वे अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में अर्पित न कर दें या उसे ऐसे अधिकार नहीं सौंपे जो उसे यह अधिकार दें कि वह उनके संस्थानों को नष्ट करने में सक्षम हो।
उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले किसी महान व्यक्ति की महानता के सामने झुकने में कुछ भी गलत नहीं लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में भक्ति या नायक पूजा की परंपरा किसी भी अन्य देश से अधिक है और यह रास्ता निश्चित रूप से अवनति और फिर तानाशाही की ओर ले जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र के रूप में विकसित करनाहोगा। यहां सामाजिक लोकतंत्र से उनका तात्पर्य था- स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों को अपनाना। वह मानते थे कि ये तीनों मूल्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुएहैं और एक के बिना दूसरे को हासिल नहीं किया जा सकता है। इनमें से एक की भीअनुपस्थिति सामाजिक लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास को विफल कर देगी।