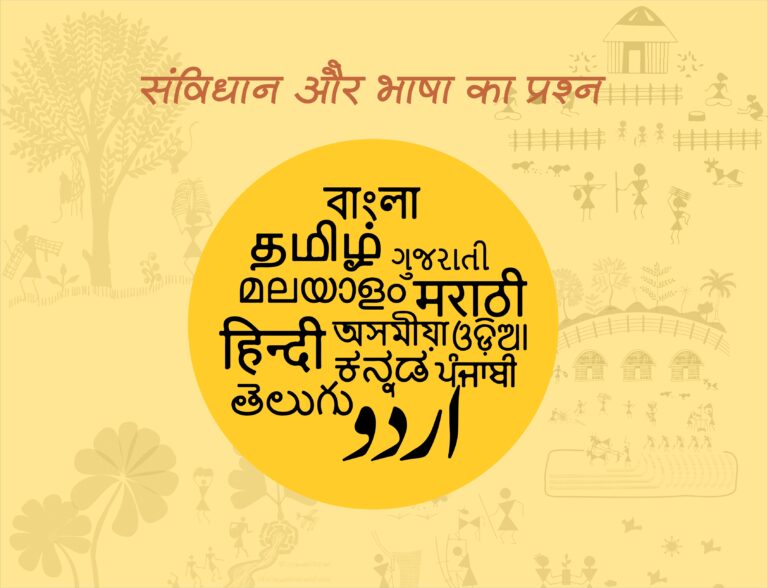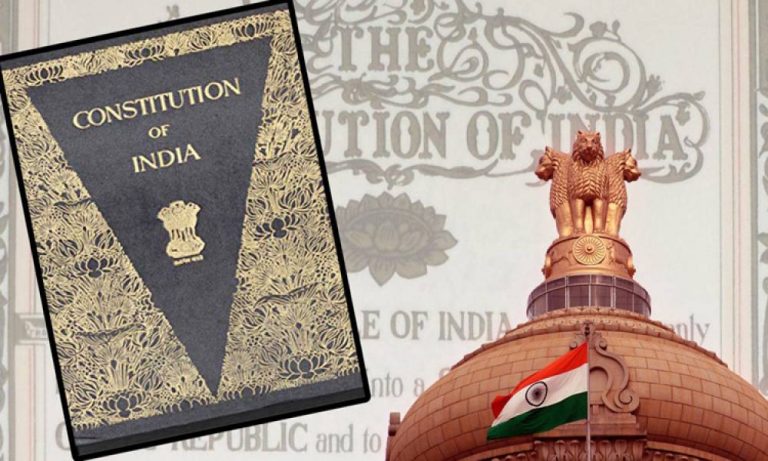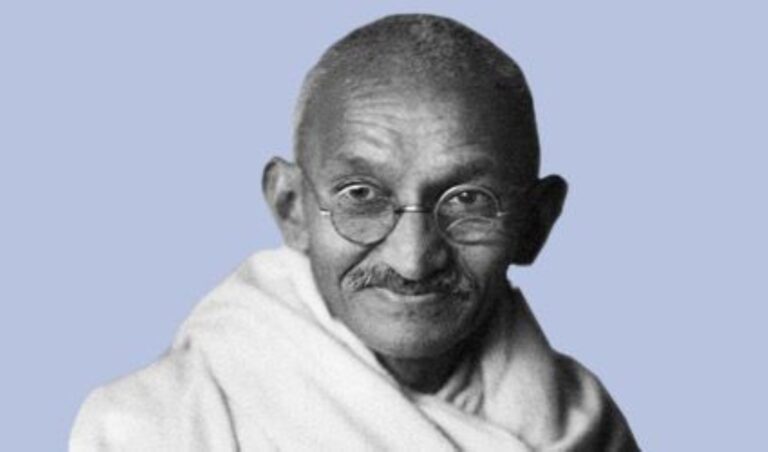मतदान: सत्ता में भागीदारी का पहला कदम
आम जनता के लिए यह समझना आवश्यक है कि सत्ता में भागीदारी का रास्ता मतदान से होकर ही निकलता है। हर पांच वर्ष में हमें अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलता है। हमारा मत ही यह सुनिश्चित करता है कि कौन सरकार बनाएगा? हम अपने मत के माध्यम से यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन हमारा प्रतिनिधित्व करे। हम राजनीतिक दलों की नीतियों और नेताओं के क्रियाकलाप के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि किसे मत देकर विजयी बनाना है। यह कहना सही होगा कि सत्ता में भागीदारी का पहला कदम मतदान है। संविधान सभा में भी इस विषय पर रोचक बहस हुई थी जो इस विषय को संविधान निर्माताओं की दृष्टि से देखने का अवसर देती है।


सचिन कुमार जैन
संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।
अक्टूबर 1949 में भारत के संविधान की उद्देशिका को अंतिम रूप देने संबंधी बहस संविधान सभा में चल रही थी। बहस में एक बात यह भी कही जा रही थी कि भारत की राज्य व्यवस्था को कोई भी शक्ति और अधिकार जनता से ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि भारत के लोग अपने मत (वोट) के जरिये राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को उनकी नीतियों और विचारों के आधार पर चुनेंगे। जिन्हें ज्यादातर जनता मत (वोट) देगी, उन्हें क़ानून, नीतियां और नियम बनाने-शासन का अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह सरकार को भी व्यवस्था चलाने के लिए जनता, वस्तुओं और सेवाओं पर कर तथा शुल्क लगाने का अधिकार मिल जायेगा।
इसके एवज़ में संवैधानिक स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका) से यह अपेक्षा की गयी कि वे भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया था- “भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय…..प्राप्त करने के लिए”; तब बहस के दौरान ब्रजेश्वर प्रसाद ने उद्देशिका में ‘संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न’ शब्दों पर आपत्ति की। उनका तर्क था कि किसी विधि संबंधी विचारधारा का वास्तविक तथ्यों से कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो उस विचारधारा का कुछ भी मूल्य नहीं है। नेपाल सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और वह अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकती है, सोवियत रूस की सरकार को रूस के साम्यवादी पक्ष को ख़त्म करने की स्वतंत्रता है….इस तरह के कामों का परिणाम क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता युद्ध की ओर ले जाती है और वह साम्राज्यवाद का कारण बनती है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है।
जनता की सर्वोच्चता पर नेहरू के विचार
जनता ही राज्य को शक्ति प्रदान करेगी, यह विचार संविधान सभा में कई लोगों, खासकर रियासतों के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य नहीं था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चली बहस का जवाब देते हुए कहा था, “जनता के सर्व सत्ता संपन्न होने की कल्पना संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में की गयी है, वह कुछ नरेशों को पसंद नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मंत्री यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन पद्धति की तीव्र निंदा के लिए उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति चाहे उसका दर्ज़ा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह कहना कि ईश्वरदत्त विशेषाधिकार से मैं मनुष्य पर शासन करने आया हूं, यह नितांत जघन्य है।”
श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ‘संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न’ शब्द रखे जाने के समर्थन में कहा कि यदि ये शब्द नहीं हैं तो हम केवल इस बात से संतुष्ट होंगे कि जनता पांच वर्ष में केवल एक बार निर्वाचन स्थल पर मत देने जायेगी इसलिए उसकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता सुरक्षित है।
महावीर त्यागी ने कहा था कि ये शब्द इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि कोई विचारधारा स्थायी नहीं होगी, किसी विचार की सरकार आयेगी और जायेगी, किंतु जनता तो रहेगी ही। भारत में लोग तो रहेंगे ही और भारत के लोगों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता निहित रहेगी। सरकार केवल जनता की प्रतीक है।
केंद्र और राज्य के सदनों के सदस्यों के निर्वाचन को संविधान में एक बहुत संवेदनशील और जिम्मेदारी का काम माना गया है। बहस-मुबाहिसे के बाद डॉ. अम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार के विषय पर प्रस्ताव पेश किया कि “लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, तथा जो ऐसी तिथि पर जो समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिए नियत की गयी हो, 21 वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अयोग्य नहीं किया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा।”
ब्रजेश्वर प्रसाद का कहना था कि “वयस्क मताधिकार में यह पूर्व धारणा होती है कि निर्वाचकगण समझदार है, जहां निर्वाचकगण विवेकशील न हों, वहां संसदमूलक लोकतंत्र नहीं हो सकता।” इस बहस से यह पता चलता है कि नागरिक के विवेकशील हुए बिना यह व्यवस्था जीवंत नहीं होगी।
इतने दशकों बाद भी संभवतः यही सवाल पूछा जा रहा है कि निर्वाचन में अंतत: मतदाता किस विवेक का इस्तेमाल करते हैं? क्या वे संवैधानिक मूल्यों को अपने निर्णय में शामिल करते हैं? हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि आज़ादी के बाद संवैधानिक नागरिकता के शिक्षा से ज्यादा विभेदकारी राजनीतिक शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिससे भारतीय लोकतंत्र का सबसे अहम किरदार ‘मतदाता’ सबसे उदासीन किरदार बन गया है। हम देख रहे हैं कि भारत के चुनावों में मतदाताओं की रूचि कम हो रही है और अब यह विचार किया जाने लगा है कि ‘मतदान’ को एक अनिवार्य कानूनी कृत्य बना देना चाहिए। सवाल यह है कि अनिवार्य कृत्य होने के बाद भी क्या मतदाता ‘विवेक और समाज हित’ का उपयोग करके मतदान करेंगे! विवेक का तो क़ानून की बाध्यता से पालन नहीं करवाया जा सकता है।
जिस दिन से संविधान बनाने के प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से आज़ाद भारत के स्वरूप का निर्धारण होने लगा था। शुरुआती दिनों में ही यह घोषणा कर दी गयी थी कि भारत में अब अस्पृश्यता नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, समाज के वंचित तबकों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा, भारत में केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं होगा, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होगा। एक तरफ तो संविधान सभा भीतरी व्यवस्था के लिए विधान बना रही थी, साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से घोषणा कर रही थी कि न तो देश के भीतर किसी समुदाय को गुलाम बनाया जाएगा, न ही भारत किसी अन्य देश के साथ हिंसात्मक या उपनिवेशवादी व्यवहार करेगा। हम विश्व में शांति चाहते हैं।
आचार्य जे.बी. कृपलानी ने 17 अक्टूबर 1949 को लोकतंत्र की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कहा था कि “लोकतंत्र क्या है? उसमें मानव समता का भाव निहित है, उसमें बंधुता का भाव निहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अहिंसा के महान सिद्धांत का भाव निहित है। जहां हिंसा है, वहां लोकतंत्र कैसे हो सकता है? लोकतंत्र की साधारण परिभाषा ही यह है कि सिर तोड़ने की अपेक्षा हम सिर गिनते हैं। हम लोकतंत्र को केवल एक संवैधानिक और औपचारिक योजना के रूप में स्वीकार करेंगे, तो असफल होंगे। भारत को लोकतंत्र के नैतिक, अध्यात्मिक और गहन भाव को समझ लेना चाहिए। यदि नहीं समझा तो हम असफल होंगे। यदि नहीं समझे तो यह पहले स्वैरतंत्र (तानाशाही व्यवस्था) बनेगा, फिर साम्राज्यतंत्र बना दिया जाएगा।”
संविधान की बहस के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर लिए गया था कि इन्हें हासिल करने के लिए हर तरह की व्यवस्था संविधान में दर्ज की जायेगी। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि राजनैतिक न्याय (जिसे डॉ. अम्बेडकर ने एक व्यक्ति, एक मत के रूप में भी परिभाषित किया) के बिना ऐसी नीतियां और व्यवस्था नहीं बन पाएगी, जिनसे आर्थिक और सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल हो सके। मतलब साफ़ था कि विभिन्न विचारधाराएं सामाजिक-आर्थिक-राष्ट्र हित के पहलुओं पर अपने तर्कों और भविष्य की योजनाओं के साथ राजनीतिक इकाई के रूप में जनता के बीच जायेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। इस आधार पर जनता अपने ‘मत’ से उनका चुनाव करेगी। इसका मतलब है कि जो दल सरकार बनायेगा, उसे अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए जनता से ही अनुमति और शक्ति प्राप्त हो रही है। अब प्रश्न यह है कि जनता किस विचारधारा को चुनती है और क्यों? यदि समाज में व्यापक स्तर पर नागरिकता, मानव हित, बंधुता और इंसाफ के पाठ शिक्षा का मूल आधार बनते, तो संभवतः जातिवादी-साम्प्रदायिक और वर्गवादी व्यवस्था की धार कम होती जाती और भारत की राज्य व्यवस्था वास्तविक रूप में मानवतावादी और लोकतांत्रिक बन पाती; लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
संविधान सभा इस तथ्य से भलीभांति परिचित थी कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न बन जाए, किंतु यदि उसे लागू करने वाले (मुख्य रूप से वे लोग, जिन्हें जनता चुनेगी) लोग खराब हुए, तो हालात बुरे होते जायेंगे। आचार्य कृपलानी ने इसी दिन कहा था कि हमें स्वयं अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि हम जनता के सेवक हैं। एक मंत्री ‘हमारी सरकार’ कहता है, ‘जनता की सरकार’ नहीं कहता। प्रधानमंत्री भी मेरी सरकार कहता है, जनता की सरकार नहीं।
प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा था कि वास्तव में यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि एक समय इसका उल्लेख मूल अधिकारों के अध्याय में ही करने का विचार किया गया था। उद्देश्य यह है कि संविधान में वयस्क मताधिकार की ही गारंटी न दी जाए, बल्कि उसे यथोचित रूप से व्यवहार में लाने की भी गारंटी दी जाए। ऐसी बात डॉ. अम्बेडकर ने भी कही थी कि निर्वाचनों को स्वतंत्र रूप से करना तथा विधान-मंडलों के निर्वाचन में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न होने देना एक मूल अधिकार है।
सवाल यह था कि सदियों से जाति-दासत्व की व्यवस्था में रहते हुए उत्पन्न हुई जड़ता और उदासीनता की अवस्था से भारत की नागरिकों को मुक्त कैसे कराया जायेगा? महज़ संविधान में लिख देने से भारत में लोकतंत्र, समानता, बंधुता और न्याय का अवतरण तो होना नहीं था। अंग्रेजों के चले जाने मात्र से लोगों को यह विश्वास नहीं होने वाला था कि वे भी स्वतंत्र हो गए हैं और अब जो व्यवस्था बनेगी, उसमें उनकी बराबरी की प्रभावी भागीदारी होगी।
सच तो यह था कि अंग्रेजों का जाना, सादृश्य गुलामी से मुक्ति थी, जबकि भीतरी गुलामी से मुक्ति का मार्ग राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना से होकर जाने वाला था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया। आज हम मतदान को एक साधारण की औपचारिक राजनीतिक आहूति के रूप में देखते हैं, किंतु सच तो यह है कि भारत के संविधान को लागू करने वाले लोगों का चयन इसी पद्धति से होना होता है। जिनके बारे में डॉ. अम्बेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यदि संविधान लागू करने वाले लोग अच्छे हुए, तो हमारा सपना साकार होगा, अन्यथा कितना ही अच्छा संविधान बना लीजिये, भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। संविधान सभा के सदस्य मानते थे कि केवल वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर देने से बात नहीं बनेगी।