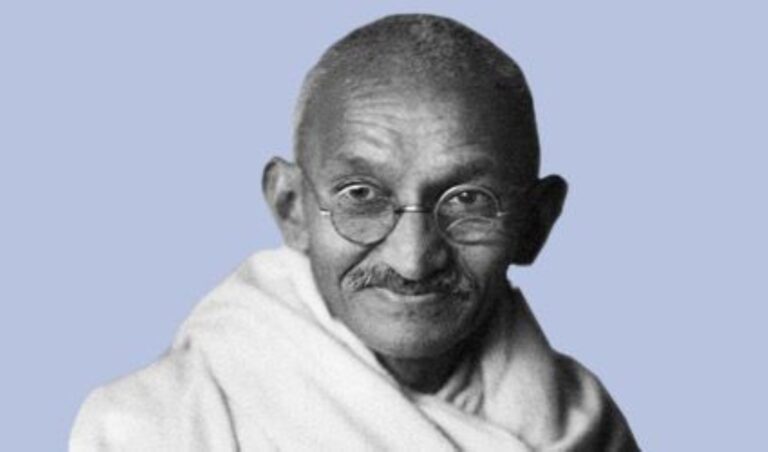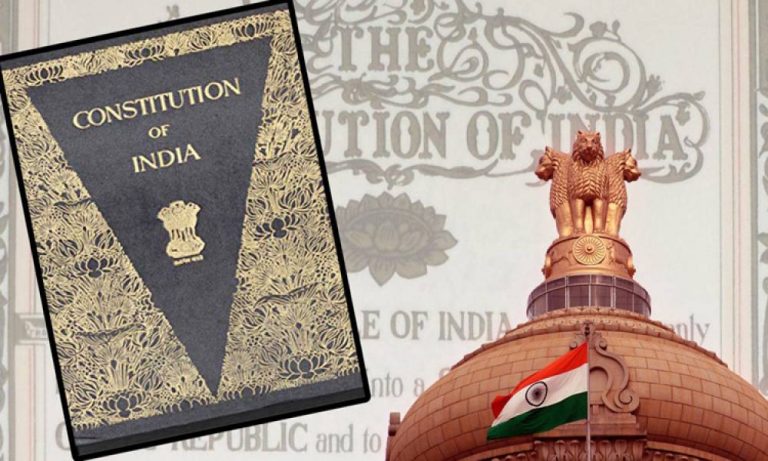समान नागरिक संहिता – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
इन दिनों देश में समान नागरिक संहिता को लेकर नये सिरे से बहस शुरू है। ताजा चर्चाओं के पीछे राजनैतिक वजहें हैं लेकिन देश में समान नागरिक संहिता को अपनाने की चर्चा कोई नई नहीं है। इसकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। ब्रिटिश शासन में जब भारत की एक ठोस पहचान नहीं थी और वह अलग-अलग रियासतों में बंटा हुआ था तब से शुरू हुई समान कानूनों की मांग ने एक लंबा सफर तय किया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित आलेखों की शृंखला की पहली कड़ी में जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में।


सचिन कुमार जैन
संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।
समान नागरिक संहिता भारतीय समाज में विभिन्न सम्प्रदायों में परम्पराओं और धर्म संबंधी पुस्तकों के आधार पर संचालित होने वाले निजी कानूनों का स्थान लेने वाली संहिता है। इनमें मुख्य रूप से विवाह, तलाक/विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण-पोषण से सम्बंधित सार्वजनिक नियम और व्यवस्थाएं शामिल हैं। सवाल यह भी है कि आखिर समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों महसूस की जाती है? वर्तमान राजनीति प्रेरित चर्चाओं से इतर इसकी लगभग 200 वर्ष लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।
सन 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसका लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को व्यवस्थित करना। 1835 में इसी अधिनियम के तहत पहले विधि आयोग (लॉ कमीशन) की स्थापना की गयी। इसके अध्यक्ष लार्ड मैकाले थे। इसी आयोग ने “लेक्स लोकी रिपोर्ट” प्रस्तुत की थी। दरअसल, एंग्लो-भारतीय लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की अदालत में ऐसी शिकायतें दर्ज की थीं कि उन पर लागू होने वाले नागरिक क़ानूनों में स्पष्टता और एकरूपता नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट के कानूनों में कुछ हद तक स्पष्टता है। तत्कालीन भारतीय प्रांतों में ईसाइयों, ब्रिटिश भारतीयों, पारसियों, पुर्तगालियों, अमेरिकियों पर लागू होने वाले कोई क़ानून नहीं थे, क्योंकि भारत एक इकाई नहीं, बल्कि कई रियासतों और साम्राज्यों में विभाजित देश था। यहां अलग-अलग राज्यों-रियासतों-साम्राज्यों के अपने-अपने कायदे क़ानून थे या फिर समुदायों के निजी क़ानून चल रहे थे। न तो कोई विधानसभाएं थीं, न ही संसद; जो एकरूप क़ानून बनाने के लिए अधिकृत होतीं।
अदालतों के सामने जो मामले आते उनमें वे संबंधित व्यक्तियों के देशों या उनके पूर्वजों के देशों के मूल क़ानून के आधार पर निर्णय करती थीं। इस तरह की न्यायिक व्यवस्था बहुत समस्याएं पैदा कर रही थी। कानूनी जटिलता से भरे इस प्रश्न के समाधान की जिम्मेदारी पहले विधि आयोग को सौंपी गयी। उस समय भारत के प्रान्तों की अदालतों में हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के निजी क़ानून (पर्सनल लॉ) के आधार पर न्यायिक प्रक्रियाएं संचालित होती थीं।
लेक्स-लोकी रिपोर्ट
अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था ने अपने नियंत्रण को “संस्थागत” रूप देने के लिए ऐसे क़ानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जो सब पर समान रूप से लागू हों। इसी प्रक्रिया में अक्टूबर 1840 में ‘द लेक्स लोकी’ रिपोर्ट आई। लेक्स लोकी का अर्थ है ‘देश का क़ानून’ या ‘स्थानीय क़ानून’ (लॉ ऑफ द लैंड)। इसने अपराधों, सबूतों/साक्ष्यों और अनुबंधों से सम्बंधित कानूनों में समानता लाने के लिए एक क़ानून बनाने की अनुशंसा की। लेकिन साथ ही रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया कि हिन्दुओं और मुसलमानों के निजी क़ानून इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। यह सुझाव मान लिया गया। हिन्दुओं और मुस्लिमों के निजी क़ानून स्थानीय न्यायालयों और पंचायतों में स्वीकार्य रहे, यानी उनके आधार पर निर्णय हुए। आमतौर पर ये कानूनी मामले एक ही समुदाय/धर्म के दो लोगों के बीच हुआ करते थे। यह तय था कि राज्य ऐसे मामलों में तब ही दखल देगा, जब कोई विशेष स्थिति बने। ब्रिटिश सत्ता ने भारत के लोगों को अपने मामले खुद निपटाने के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था चलाने की छूट दी थी। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद रणनीतिक रूप से वर्ष 1859 में ब्रिटेन की महारानी ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन की राज व्यवस्था भारत के धर्म समुदायों के “निजी मामलों-कानूनों” में दखल नहीं देगी। इनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और धार्मिक व्यवहार शामिल थे। इसके दूसरी तरफ जमीन, साक्ष्य, अनुबंध और आपराधिक मामले ब्रिटिश शासन के कानूनों से संचालित होते थे।
पारंपरिक कानूनों की सीमा
एक समस्या यह भी थी कि एक सम्प्रदाय के शास्त्रों में लिखी बात उसके सभी समूहों में एकरूप से लागू हो, ऐसा भी नहीं होता। मसलन जाट और द्रविड़ समुदायों में टकराव रहा। हिन्दू क़ानून के उलट शूद्रों में विधवा विवाह की अनुमति थी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने “हिन्दू क़ानून” को अपने निर्णयों का आधार बनाया क्योंकि उन्हें भय था कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें “ब्राह्मण प्रभुत्व” के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह भी समझ आया कि हिन्दू कोई एक समान इकाई नहीं है, इसमें कई समुदाय हैं, उनके अपने अपने क़ानून हैं और हर मामले में अगर हर समुदाय के पारंपरिक कानूनों/नियमों का अध्ययन करेंगे, तो न्यायधीश परेशान हो जायेंगे। अतः सहूलियत के लिए एक ही धार्मिक क़ानून को मान लिया गया।
शरिया क़ानून ब्रिटिश शासन की व्यवस्था में उतनी गहराई से नहीं लागू हुआ, जितना हिन्दू क़ानून हुआ। ऐसे में शरिया क़ानून के बजाय पारंपरिक मुस्लिम क़ानून अपनाए जाने लगे। ये क़ानून महिलाओं के लिए और ज्यादा भेदभावकारी थे। शरिया क़ानून महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार की भी बात करता है और मेहर/आर्थिक आधार पर व्यवस्थापन की भी; लेकिन पारंपरिक नियम ऐसी व्यवस्था नहीं करते। इसके बाद मुस्लिम समुदाय में दबाव बनने लगा और वर्ष 1937 में शरियत क़ानून पारित हुआ। लेकिन इसके बाद उसमें भी जरूरी संशोधन नहीं हुए।
पारंपरिक हिंदू कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है। इन कानूनों में महिलाओं को उत्तराधिकार, पुनर्विवाह और तलाक के अधिकार नहीं दिए गये। इसके कारण विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उनकी बेटियों की स्थिति बहुत खराब रही है।
हम जानते हैं कि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए क़ानून बनवाने की पहल की, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधियों को भी यह भय सताता था, कि इससे हिन्दू समाज के सूत्रधार नेता नाराज़ हो जायेंगे। कुछ कानूनी सुधार की कोशिशें की जाती रहीं; मसलन विधवा हिन्दू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विवाहित महिला की संपत्ति अधिनियम, 1923 और हिन्दू उतराधिकार (विसंगतियों की समाप्ति) अधिनियम 1928 बना। इसके साथ की बहुत कठिनाइयों के बाद वर्ष 1865 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बना। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को संरक्षण देने वाला यह पहला क़ानून था। भारतीय विवाह अधिनियम 1864 बना, लेकिन यह केवल ईसाई समुदाय पर लागू होता था।
सामाजिक चेतना
अखिल भारतीय महिला परिषद ने पुरुषों के प्रभुत्व वाली शासन व्यवस्था और विधायिका पर गहरा असंतोष जाहिर किया। परिषद के वर्ष 1933 के सम्मलेन में लक्ष्मी मेनन ने कहा कि यदि हमें अदालत में तलाक लेना है, तो हमें यह कहना होगा कि हम हिन्दू नहीं हैं, हम हिन्दू क़ानून से बंधे हुए नहीं हैं। पुरुषों से भरी हुई विधान परिषद कभी भी व्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव नहीं आने देगी, जो हमारे लिए (महिलाओं के लिये) लाभदायी होंगे।” कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी लैंगिक समानता लाने के लिए समान नागरिक संहिता लाने की मांग की गयी थी, जो निजी कानूनों का स्थान ले।
इसके बाद वर्ष 1937 में हिन्दू महिला के संपत्ति के अधिकार का क़ानून बना। जिसे देशमुख बिल भी कहा जाता है। इसके बाद बी. एन. राउ समिति गठित हुई। जिसे यह समझना था कि समान हिन्दू कानूनों की आवश्यकता क्या है? इस समिति ने भी कहा कि यह वक्त समान नागरिक संहिता को लागू करने का है। यह संहिता महिलाओं को समान अधिकार दिला सकेगी, लेकिन इस समिति का ध्यान मुख्य रूप से हिन्दू निजी कानूनों में सुधार पर ही था।
भारतीय नागरिकों को विवाह का अधिकार दिलाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम वर्ष 1872 में बना था। लेकिन इसके तहत व्यक्ति को अपने धर्म की घोषणा करनी होती थी और केवल इस क़ानून के तहत हिन्दू ही विवाह कर सकते थे। वर्ष 1923 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ और इस संशोधन के मुताबिक़ बौद्ध, सिख और जैन भी विवाह कर सकते थे और उन्हें अपने धर्म की घोषणा करने की बाध्यता नहीं थी।
संविधान सभा में भी यह विषय चर्चा का केंद्र रहा। संविधान प्रारूप समिति ने अनुच्छेद 35 के रूप में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रावधान रखा। जो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के रूप में शामिल हुआ। समान नागरिक संहिता बनाने के लिए सरकार को बाध्य नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक नीति के विषय के रूप में शामिल किया गया। सभा के कई सदस्य, जिनमें मोहम्मद इस्माइल साहब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग बहादुर शामिल थे, यह मान रहे थे कि भारत में हर समुदाय के अपने परंपरागत कायदे-नियम हैं। उन समुदायों के लोग उन्हें धार्मिक नियम मानते हैं, ऐसे में यह अपेक्षा करना उचित नहीं है कि बिना उन्हें समझाए समान नागरिक संहिता आकार ले सकेगी। समाज से संवाद करके ही इसे लागू किया जा सकता है। अतः इस विषय को तत्काल लागू न किया जाए, बल्कि समाज का उन्मुखीकरण करके इसे लागू किया जाए।
जवाहर लाल नेहरु, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और के. एम. मुंशी समान नागरिक संहिता के समर्थक थे, लेकिन उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था।
स्वतंत्र भारत की विधान परिषद और संसद में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव लाने की कोशिशें हुईं और डॉ. अम्बेडकर को इसे प्रस्तुत करना था, लेकिन हिन्दू व्यवस्था के प्रति उनकी मुखरता के चलते यह विषय साझा सहमति हासिल नहीं कर पाया। हिन्दू कोड बिल पर भी बहुत बहस हुई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसका विरोध किया। हिन्दू कोड बिल का मकसद पारंपरिक कानूनों के कारण पैदा हुए भेदभाव को कम करना था, लेकिन इसे हिन्दू विरोधी और भारत विरोधी कहा गया। लम्बी जद्दोजहद के बाद वर्ष 1956 में चार क़ानून पारित हुए – हिन्दू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम।
समान नागरिक संहिता को पंथ-निरपेक्षता, नागरिक-व्यक्ति के शोषण से मुक्त होने, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के साथ-साथ व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के नज़रिये से महत्वपूर्ण माना जाता है। शाहबानो (वर्ष 1985-86) मामले के न्यायिक निर्णय से यह एक बार फिर से चर्चा में आई। इसे बहस के केंद्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ लाए थे, जिनमें एकतरफ़ा तलाक की अनुमति रही है। इस मामले से यह “पहचान की राजनीति” का विषय बन गया। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत किया गया जो पत्नी, बच्चों और पालकों के पालन-पोषण से सम्बंधित प्रावधान करती है। वर्ष 1986 में मुस्लिम (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम बनाया। इसमें अपराध संहिता के इस प्रावधान को मुस्लिम पहचान के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया और तत्कालीन भारत सरकार ने संसद में क़ानून में संशोधन कर दिया कि अपराध संहिता का यह प्रावधान मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा। तीन तलाक के मसले पर वर्ष 2019 में इसी क़ानून में संशोधन किया गया है।
समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण नीतिगत और संवैधानिक पहल है, लेकिन जैसा कि माना जाता रहा है कि इस विषय पर समाज के साथ संवाद होना बहुत जरूरी है। अगर तार्किक ढंग से समानता और गरिमा की दिशा में बढ़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से इस संहिता को समाज की सहमति से ही आकार देना आसान हो जाएगा।